Last Updated on: 16th July 2025, 01:15 pm
बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लामेन्ट में। पान सिंह तोमर (Paan Singh Tomar) का ये डायलॉग फ़ेसबुक की दीवारों पे बहुत दिनों से छाया हुआ था। तिग्मांशु धूलिया (Tigmanshu Dhuliya) की हासिल देखने के बाद उनकी इस फ़िल्म से उम्मीदें महीनों पहले से बाँध ली थी। आज पवई आईआईटी के पड़ौसी बिग सिनेमा के थियेटर में फ़िल्म देखने के बाद लगा जैसे कोई साध पूरी हो गई।
एक बागी के लिये इतना सम्मान, और अपने सिनेमा के लिये इतना प्यार, इतना दुलार, बड़े अरसे बाद आया। फ़िल्म शुरु होने से ठीक पहले परदे पर कुछ बच्चों के इशारों से देश के सम्मान के प्रतीक राष्ट्रगान को फ़िल्म के भावी दर्शक जिस तन्मयता से सुन रहे थे ठीक वही भावना फ़िल्म के बाद पता नहीं क्या होने के लिये रुके एंड क्रेडिट को भरपूर निहारते दर्शकों के भीतर महसूस हो रही थी.
जे बात को जवाब कौन देगो
आज बहुत समय बाद किसी फ़िल्म के लिये दर्शकों के व्यवहार को देखकर लगा कि फ़िल्म का असर सचमुच कोई चीज़ होती है। कैसे लोग मानना ही नहीं चाहते कि फ़िल्म पूरी हो गई है। चीज़ें जैसे स्लो-मोशन में होने लगती हैं। लोग कुछ देर के लिये फ़िल्म में दिखाई गई दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहते। फ़िल्म देखते हुए वो कुछ घंटों के लिये फ़िल्म में ही कहीं छुपा हुआ पात्र हो जाते हैं। पान सिंह तोमर को देखने के बाद यही सब होता देख अच्छा लगता है।
पान सिंह तोमर में यकीनन मैलोड्रामाटिक मूमेंट बहुत सारे हैं। छुटटी पर आये एक फौजी का पत्नी के नजदीक आने के लिये बच्चों को ‘लैमनचूस’ लेने दूर वाली दुकान पे भेजना, माँ की गाली देने पर उस फौजी का अपने कोच को टोकना, अपने ऑफिसर से कहना कि वो अपने सारे अफसरों के आदेश इसलिये नहीं मान सकता क्योंकि वो इस लायक नहीं हैं, एक खिलाड़ी होने के नाते जंग में न जाने देने पर अपने गुस्से को भट्टी में झोंकना, भैंसे पर बैठे एक सिर मुंडाये लड़के को बागियों की सेना का यमराज समझ लेना, अपने भाई के मर जाने के बाद माँ की चूडि़यों को यादकर उसकी लाश से पूछना कि ‘जे बात को जवाब कौन देगो’ या फिर अंत में एक बागी का गोलियां लग जाने के बाद मौत से ठीक पहले खेल का मैदान, दर्शकों की तालियां, और अपनी पत्नी की झलकियां देखना, ये सबकुछ कई हद तक बहुत इमोश्नल या मैलोड्रामाटिक ज़रूर लगता है, पर फ़िल्म की एक लयात्मक गति में अपनी अपनी जगह पर ये सब कुछ फिट सा बैठ जाता है। फ़िल्म का सुर इससे कहीं नहीं बिगड़ता, ये सब कहीं ओवर द टॉप नहीं लगता।
इरफ़ान ख़ान का ज़बरदस्त अभिनय
फ़िल्म की पूरी कहानी इतनी सरलता से बहती है कि कोई झोल नज़र नहीं आता। इंटरनैशनल सिनेमा का एक्सपोज़र अक्सर अपनी फ़िल्मों से उन्हें कम्पेयर करने पर मजबूर करता है और आंकने पर ज्यादातर अपनी फ़िल्में कमज़ोर नज़र आती हैं पर इस फ़िल्म को देखते हुए वो कमजोरी नज़र नहीं आती। फ़िल्म अपने वक्त के बहुत करीब खड़ी नज़र आती है। कहीं नकली या बनावटी नहीं लगती। किरदारों के व्यवहार और भाषा दोनों ही कहानी में अपनी जगह बनाये रखते हैं, कहीं कोई मिसमैच नहीं लगता।
फ़िल्म देखने से ठीक पहले फ़िल्म के पटकथा लेखक संजय चौहान की कही बात पढ़ी थी कि माही गिल को बुंदेलखंडी भाषा सीखने में कुछ दिक्कत हुई थी लेकिन फ़िल्म में उनका मेकअप और उनकी संवाद अदायगी दोनों से ही वो चंबल की घाटी की ही कोई असल औरत लगती हैं।
इरफान खान तो खैर इस फ़िल्म के बाद अपनी बेहतरीन अदायगी के कुछ और पायदान चढ़ ही गये हैं। बॉलीवुड के साथ साथ वर्ल्ड सिनेमा में भी उनकी अपनी अलग पहचान बन ही चुकी है। उनकी सबसे अच्छी बात यही है कि वो किसी भी फ़िल्म में स्टार नहीं होते, वो हर फ़िल्म में अपने साधारण से व्यक्तित्व को उनको मिले किरदार में उतने ही साधारण तरीके से ढ़ाल लेते हैं।
पान सिंह तोमर जो थोड़ा नादान भी है, झुकता भी है, शरारत भी करता है, जज्बाती भी है, और जब दौड़ता है तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर। इस बात की परवाह किये बिना कि नम्बर कौन सा आयेगा। धावक, प्रेमी, फौजी, बागी, पिता, और लीडर हर रुप में खुद को ढ़ाल लेने वाले एक साधारण से इन्सान के बहुआयामी किरदार में इरफान हर एंगल से फिट लगते हैं।
शहर के दर्शकों को गाँव की कहानियों से जोड़ते तिग्मांशु धूलिया
पान सिंह तोमर देखकर लगता है कि तिग्मांशु धूलिया मौजूदा समय के ऐसे चंद निर्देशकों में से एक हैं जिनकी फ़िल्मी कहानियों में अपनी मिट्टी की महक है, जिसके किरदार नकली नहीं लगते।
जिनकी फ़िल्मों को रॉकस्टार जैसी फ़िल्मों की तरह एक फ़ैशनेबल स्टार और बेहतरीन म्यूजिक की बैसाखी की ज़रुरत नहीं पड़ती। जिनकी कहानियों और किरदारों में वो ईमानदारी है कि हर आदमी उससे रिलेट कर पाता है। शायद वैसा ही कोई किरदार हर किसी ने कभी न कभी अपने आस पास देखा होता है, वैसी ही कोई कहानी उस किरदार से सुनी होती है। तिग्मांशू उसे समेटकर बस फ़िल्म के रुप में सहेज लाते हैं।
पान सिंह तोमर अपनी उस व्यवस्था पर व्यंग्य भी करती है जिसमें योग्यता प्रभावशाली लोगों की अज्ञानता के बीच कहीं दब जाती है। एक आम इन्सान जो समाज और कानून के दायरे में रहकर काम करता है उसे कुचल दिया जाता है और वही इन्सान जब शक्ति का संतुलन अपने हाथों में ले लेता है तो उसे बागी घोषित कर दिया जाता है।
फ़िल्म बागी और डकैत का अन्तर बताते हुए एक तर्कपूर्ण पौलिटिकल स्टेटमेंट रखती है और उसे पूरी तरह जस्टिफाई भी करती है। इस दोषपूर्ण व्यवस्था में अपनी बात सुनाने और खुद को साबित करने के लिये या तो आपको डकैत हो जाना होगा या फिर डकैती का विरोध करता हुआ एक बागी बन जाना होगा। बीच की स्थिति में आप हमेशा अस्तित्वहीन रहेंगे। इस तरह फ़िल्म एक फौल्टी सिस्टम के खिलाफ क्रान्ति के पक्ष में खड़ी नज़र आती है।
पिछले कुछ समय से निराश कर रहे अपने बॉलीवुड से पान सिंह तोमर ने एक बार फिर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। शहर के मल्टीप्लैक्सों में गाँवोंके बीहड़ की बात करती फ़िल्में मौजूदा कमर्सियल सिनेमा में एक बागी की तरह ही नज़र आती हैं। पान सिंह तोमर जैसे ही और कई बागियों की हमारे सिने संसार को बहुत दरकार है।




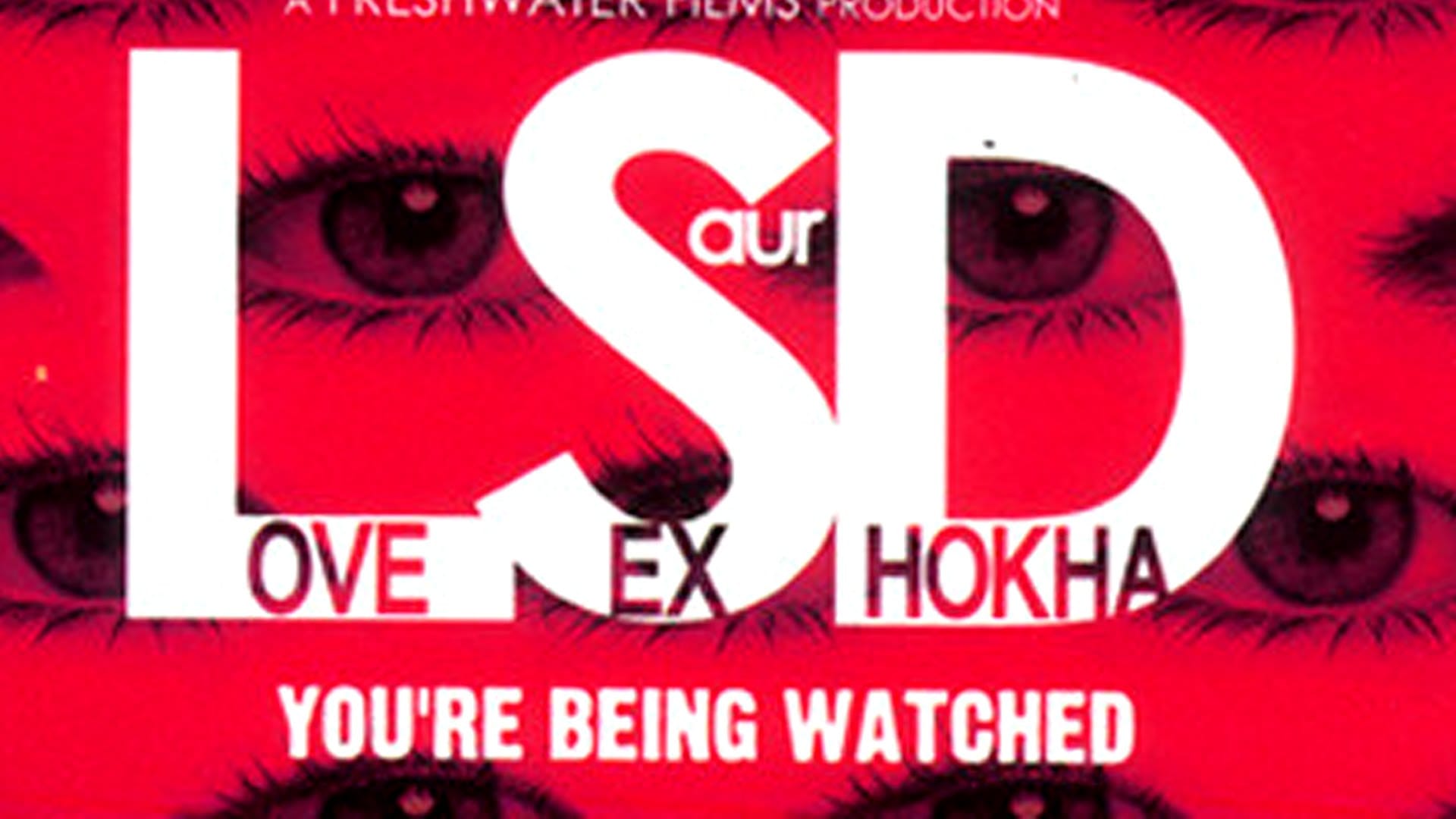
वाह बहुत ही सुंदर विश्लेषण , उमेश जी । इस पिक्चर में इरफ़ान द्वारा कहे गए ये डायलाग पहले ही आकर्षित कर रहे हैं सबको । जरूर देखेंगे , वैसे भी इरफ़ान के अभिनय के कायल तो हम हैं ही । दिलचस्प पोस्ट
Nice article ! please add a subscription button also !
Thank you
sach aaj aise hi kirdaay ki hamare rugn hote samaj ko sakht jarurat hai..
bahut badiya sarthak prastuti..